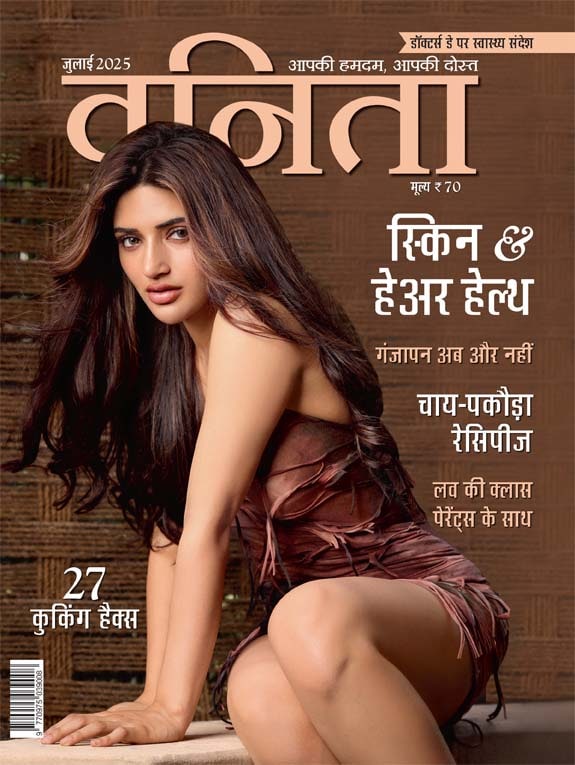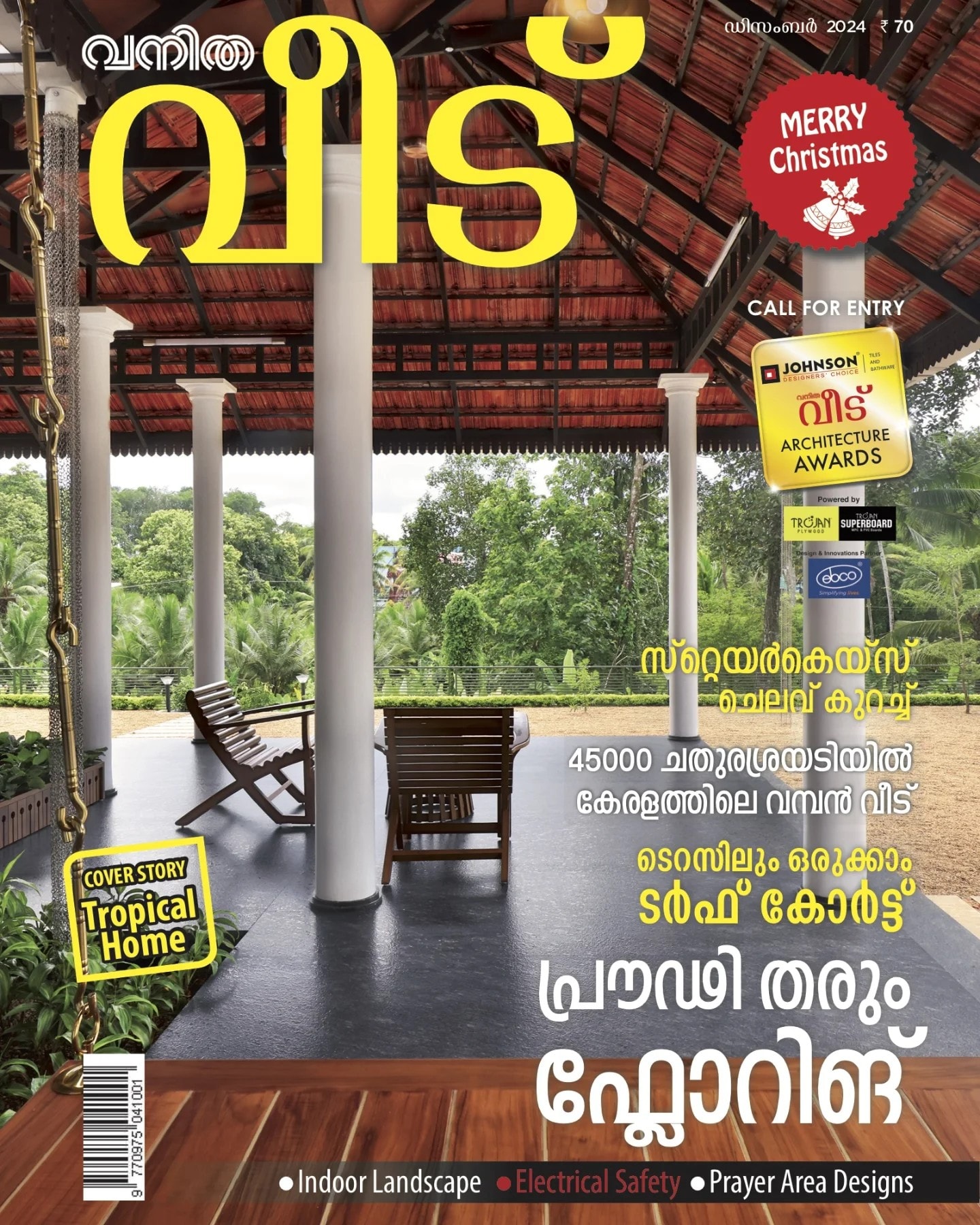सड़क के उस ओर से आता जुलूस दीनानाथ बनर्जी लेन के बायीं तरफ मुड़ गया था। ‘‘पाकिस्तान मुर्दाबाद ! मुर्दाबाद ! मुर्दाबाद!! हमसे जो टकराएगा ! चूर-चूर हो जाएगा !!’’ पारोमिता बनर्जी के कमरे की लंबी, बड़ी-बड़ी खिड़कियों के कांच भी जैसे पल-पल बढ़ते शोर की गरज से सहम गए थे। आवाजें सिर्फ ऊंची नहीं थीं, उनमें गुस्सा था, आक्रोश भी, और एक अनजाने परिणाम की चेतावनी। यों तो कलकत्ता की सड़कों पर जुलूस या प्रदर्शन होना कोई अनहोनी बात नहीं, पर ना जाने क्यों, पारोमिता बेचैन हो उठी थीं।
परदे सरका कर उन्होंने नीचे देखा। जैसा कि उम्मीद थी, नौजवान लड़कों से ले कर अधेड़ उम्र के व्यक्तियों का हुजूम, कुछेक बच्चे व औरतें भी थीं। पारोमिता ना चाहते हुए भी खिड़की पर खड़ी रहीं।
‘‘इन लोगों ने जीना दूभर कर रखा है, मां। कालीघाट के पास रामनवमी के जुलूस पर पथराव हुआ है। इसी वजह से...’’
पारोमिता ने पीछे मुड़ कर देखा। शुभोजित का गोरा, तमतमाया चेहरा नजर आया। प्रेसीडेंसी काॅलेज में प्रोफेसर, इंटरनेशनल रिलेशंस में एक जाना-माना नाम।
‘‘आप खिड़की बंद कर दीजिए। आपकी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं।’’
पारोमिता ने खिड़की तो बंद नहीं की, पर शुभोजित का बढ़ा हुआ हाथ थाम लिया था। बिस्तर पर लेट कर उन्होंने आंखें बंद कर लीं।
‘‘आप ठीक तो हैं ना !’’
‘‘आं-हां, सब ठीक है... तुम जाओ बेटे, मैं कुछ देर सोऊंगी।’’
शुभोजित ने मां के चौड़े माथे से पसीने की बूंदें पोंछीं और उठ खड़ा हुआ। खुली खिड़की बंद करके उसने परदे खींच दिए। ‘बढ़ती उम्र के साथ-साथ कितना कम बोलने लगी हैं मां,’ उसने सोचा, ‘कुछ मन में आया होगा, तो भी आसानी से बताएंगी नहीं।’ अपनी स्वयं की बढ़ती उम्र के साथ-साथ शुभोजित ने भी उनसे जिद करके कुछ पूछना छोड़ दिया था। अनुभव और उम्र ने उसे भी सिखा दिया था कि केवल पूछने मात्रा से ही सब नहीं जाना जा सकता।
प्रतीक्षा की अग्निपरीक्षा से गुजरना ही पड़ता है। पूछनेवाले को भी, बताने वाले को भी। अपने जीवन के 45 वर्षों में उसने पारोमिता को इतना तो समझ ही लिया था कि उनके हृदय के गहनतम खजाने की चाबी वह महज पुत्र होने के अधिकार से नहीं पा सकेगा। और किसी भी तरह की जिद से वह चाबी हथियाने की उसकी इच्छा नहीं थी।
अंधेरे कमरे में टेबल लैंप की रोशनी पारोमिता की मुंंदी आंखों को सहला रही थी। यह नींद भी थी, और नींद का स्वप्न भी। जाग्रत अवस्था नहीं थी, तो सुप्तावस्था भी नहीं।
‘क्यों,’ पारोमिता ने सोचा, ‘क्यों ऐसे नारों को आसानी से झेल नहीं पातीं वे। क्यों मन की सारी तहें उथल-पुथल हो कर फूहड़ हाथों से बंधी गठरी की तरह खुल-खुल जाती हैं?’
अनजाने ही आंखें और कस कर बंद कर ली पारोमिता ने। हैरत थी, बंद करते ही सारा मंजर साफ-साफ दिखायी देने लगा। ढाका, उन दिनों के ईस्ट पाकिस्तान का आबाई शहर... शहर के बाहरी छोर पर बना वह खूबसूरत, खुला सा बंगला, जिसकी ऊंची दीवारों के पार चाह कर भी नहीं झांका जा सकता था। करीब 7 बरस की थीं पारोमिता, जब वे इस घर में आए थे। 1947 के विभाजन के बाद, जब बंगाल का एक बड़ा हिस्सा ईस्ट पाकिस्तान बना, तो बंगालियों को यह चुनने की आजादी दी गयी कि वे हिंदुस्तान के साथ आना चाहेंगे या पाकिस्तान के साथ। स्वाभाविक तौर पर बंगाली हिंदुओं ने हिंदुस्तान आना चाहा। पर पारोमिता के पिता, जो रंगपुर इलाके में सब जज थे, उन्होंने किसी कारण से ढाका की तरफ जाने का निर्णय लिया।
पारोमिता को आज भी याद है सियालदह स्टेशन पर जाती हुई गाड़ियों का हुजूम, ढेरों आदमियों का रेला... एक बेहद लदे हुए कोच में दीदी मां और मां के साथ बैठी छोटी सी पारू... मां के आंसू थम ही नहीं रहे थे। वे बार-बार खिड़की से बाहर देखतीं, और आंचल से चेहरा ढांप लेतीं। आज इतने बरस बाद भी पारोमिता उन आंसुओं का सागर भूल नहीं पायी हैं। आज उन्हें लगता है कि उस आजादी के तूफान के आर-पार मां जैसे अनगिनत लोगों के आंसुओं का सागर है, जो शायद आज भी नहीं सूखा।
चिट्टागौंग में, 8 बरस की उम्र में, पहली बार स्कूल गयीं पारोमिता। यह दुनिया काफी नयी थी उनके लिए- बंगला बोलती, खुशशक्ल मुस्लिम लड़कियां, बेहद सभ्य, नम्र और प्यार करने वाली उस्तानियां। यह दुनिया पारू की नजर में सिर्फ स्कूल की दुनिया थी, हिंदू-मुसलमान होने की विसंगतियों से परे। और ऐसा भी नहीं कि मुसलमान शब्द से अनजानी रह पायी हों वे। पिता के दफ्तर के बाहर, घर पर निरंतर होती बहस, बोलचाल में, सब में यह शब्द बार-बार उभरता था। पर नन्ही पारू को शायद उस शब्द का मर्म केवल छू कर गुजर जाता था। पारू के लिए बंगला घर की भाषा थी, उर्दू और अंग्रेजी स्कूल की। यहां तक कि दीनियत की भी प्रारंभिक शिक्षा उन्हें मिली। यहां कोई ऐसी बात नहीं थी, जो उनके बालमन को झिंझोड़े। स्कूल की सखियों का साथ घर तक भी चला आता था। ना तो पारू की मां, ना ही उनकी दो प्रिय सहेलियां, फराह और फहमीदा की मां ने कभी बच्चों में भेदभाव बरता था। माछेर छोल उन्हें प्रिय था, बिरयानी पारू को, और साथ ही बढ़ रही थी किताबों की दुनिया से नजदीकियां।
टिप... टिप... टप टप... भड़भड़ भड़ाम...
छोटी-छोटी बूंदें मेघों की छाती फाड़ धरती को नहला रही थीं। काला, डरावना आसमान, पल-पल बढ़ती बारिश और नन्हे-नन्हे बस्ते सीने से चिपकाए दो सखियां, पारू और फहमीदा।
‘‘पारू, हम दौड़ कर घर पहुंच सकते हैं...’’ फहमीदा ने भीगी पलकें छपकाते हुए कहा।
‘‘पर मेरा घर तो काफी आगे है। बीच का कच्चा रास्ता फिसलन से भर गया होगा।’’
‘‘अरे मेरे घर रुक जाना ना ! शाम को परवेज भाई तुम्हें घर छोड़ आएंगे।’’
पारोमिता की गुलाबी ढाकाई साड़ी निचुड़ कर हाथों का रुमाल बन गयी थी। फहमीदा की बात मानने के सिवा कोई चारा ना था। दोनों सखियों ने बस्ते सिर पर धरे, हथेलियां कस कर थामीं, और भाग पड़ीं घर की ओर। करीब डेढ़ मील की दूरी पर बड़ी हवेली थी, खान साहब का घर, जहां पारू और फहमीदा की हंसी से गुलजार हवेली की दीवारें खिलखिलाती रहती थीं। पारू के लिए एक बड़ा जबर्दस्त आकर्षण था खान साहब की लाइब्रेरी, जो दीन-दुनिया के जाने-माने लेखकों की किताबों से अटी पड़ी थी। फहमीदा को किताबों का उतना शौक ना सही, पर पारू के साथ जब वह भी लाइब्रेरी की धूल फांकती, तो खान साहब के चेहरे पर मुस्कराहट तैर जाती। वे रिवायती मुसलमान तो थे, पर लड़कियों की शिक्षा के जबर्दस्त हिमायती। उन दिनों के कई कन्या विद्यालय और समाज-सुधार की संस्थाओं से वे जुड़े थे। पारोमिता के पिता एक जिम्मेदार ओहदे पर तो थे, पर उसके आगे या उससे परे कुछ करने की इच्छा या समय उनके पास नहीं था।
खान साहब के घर का माहौल पारू को बहुत भाता था। फहमीदा की अम्मी व फूिफयां बुर्का पहनती थीं, पर उन्हें हिजाब पसंद नहीं था, तो किसी ने उन्हें मजबूर नहीं किया था। भाई लोग पढ़ाई में भी साथ थे और खेलकूद में भी, जबकि पारू को अपने बड़े भाइयों से हमेशा एक डर सा लगता था। वे कलकत्ता में रह कर वकालत पढ़ रहे थे। घर पर कम ही आते थे। फहमीदा को वे अकसर अपने बड़े भाइयों पर हुक्म चलाते देखती थीं। कभी कोई किताब लानी हो, कहीं जाना हो, या महज दुपट्टे रंगवाने हों।
उस दिन भी जब दोनों सहेलियां घर पहुंचीं, तो परवेज भाई दरवाजे पर ही मिल गए।
‘‘भाईजान !!! जल्दी गेट खुलवाइए...’’
‘‘अरे... अंदर आओ, कितना भीग गयी हो दोनों...’’
सहमी हुई पारोमिता ने साड़ी और कस के निचोड़ी और चप्पल कोने में उतारी।
‘‘पारू...’’ फहमीदा अंदर भागते हुए चिल्लायी, ‘‘जल्दी ऊपर आओ... कपड़े बदल लेंगे।’’ सदा की बेसबर उसकी सहेली ऊपरी मंजिल तक दौड़ लगा चुकी थी।
पारू बेहद संकोच महसूस कर रही थीं, भीगे कपड़ों में। पीछे-पीछे चलते परवेज की नजरें उन्हें अपनी पीठ से चिपकी मालूम हो रही थीं।
‘‘वहां, उस तरफ, सीढ़ियों से ऊपर चली जाइए...’’
पारू को तो हवेली की हर सीढ़ी, हर कमरे का पता था, फिर भी ना जाने कदम क्यों नहीं उठ रहे थे। धीरे-धीरे चलने पर भी पैर जमे से जा रहे थे। उन्होंने पीछे मुड़ कर देखा, तो परवेज की भूरी आंखों से सामना हो गया।
काली अचकन, सफेद पाजामा, गहरी भूरी, एक्सरे सा उतारती आंखें... पारू को लगा जैसे वे वहीं गिर पड़ेंगी।
‘‘आप जल्दी चली जाएं और कपड़े बदल लें, वरना सरदी लग जाएगी...’’
परवेज की बात पर उन्होंने फिर मुड़ कर देखा- क्या यह वाकई जल्दी ओझल हो जाने की ताकीद थी... या कुछ और?
अपनी आंखों पर भी बादल सा गहराता मालूम हुआ पारू को। अबकी बार परवेज खान को कोई सलाह नहीं देनी पड़ी। हर आवाज से पल्ला छुड़ाती पारू ऊपर खट-खट सीढ़ियां चढ़ गयीं।
ठीक दो दिन बाद डिस्ट्रिक्ट सब जज नीलमणि बैनर्जी का सरकारी बंगला। खुली, पाटदार खिड़कियों पर ढके ढाकाई मलमल के परदे और चौड़े पाटदार बिस्तर पर, बुखार में तपती पारोमिता।
दीदी मां बार-बार काली मां के मंदिर से लाए पानी में रुमाल निचोड़ कर माथे पर ढकतीं, और कुछ-कुछ बुदबुदातीं। फहमीदा परवेज के साथ आयी है, सहेली की खैरियत पूछने। पारू की मां की आंखें भर आयी हैं।
‘‘दो दिन से पेट में कुछ नहीं गया... वैद्यराज की दवा भी असर नहीं कर पा रही।’’
‘‘ठाकुर मां, आप परवेज भाई को चेकअप करने दें। उनकी डॉक्टरी का आखिरी साल है। वे जरूर पारू को ठीक कर देंगे।’’
ठाकुर मां ने सिर हिला दिया था। परवेज ने नब्ज पकड़ते ही समझ लिया, निमोनिया दस्तक दे चुका है। कमजोर पारू की ठंड में जकड़ी पसलियों को संभाला अंग्रेजी दवाइयों के गरम जिरहबख्तर ने, फहमीदा के प्यार ने, और परवेज खान की नजर ने। लगभग हर रोज, शाम के 7 बजते ही निशब्द रोगिणी की आंखें द्वार से चिपक जातीं। डॉक्टर अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई समेट, बहन को ढाल बना और अदब का जामा ओढ़ साइकिल पर चला जाता। बातें होतीं फहमीदा से और नजरें झपकतीं परवेज की ओर। आधे-एक घंटे की यह डोज पारू को अगले दिन तक राह तकने का मंत्र दे जाती। पर निमोनिया को तो जाना ही था और वह जाते-जाते परवेज खान को भी साथ ले गया। पारू तो ठीक हो गयीं, और परवेज को एक अजीब बीमारी ने आ घेरा। अब जज साहब के बंगले पर रोज-रोज डाॅक्टर का क्या काम? उधर पारोमिता को कोई ऐसा थर्मामीटर ना मिल पाया था, जिसमें वह अपने दिल पर चढ़े बुखार को वजह बना, फहमीदा के भाई को बुलावा भेजतीं।
फिर एक दिन खान साहब की लाइब्रेरी में परवेज कुछ खंगालता नजर आया। पारू से अब रहा ना गया। धड़धड़ाते हुए वे गरीब डाॅक्टर के आगे जा खड़ी हुईं।
‘‘ऐसे छोड़ा जाता है मरीज को... ना कोई दवा, ना खैर-खबर... मैं मर जाती तो?’’
परवेज के होश फाख्ता की तरह उड़ गए। उसने वाकई कभी पारू को इतने करीब से नहीं देखा था। गुस्से से लाल, गेहुआं रंग चंपई रंग की साड़ी में घुलमिल गया था। उसमें से झांकती बड़ी-बड़ी जवाफूल सी लाली लिए काली आंखें।
‘‘आप... आप मर कैसे जातीं?’’ परवेज बुदबुदाया, ‘‘आप मर जातीं तो...’’
‘‘तो?’’ पारू गरजीं।
‘‘तो मैं भी मर जाता...’’ हथियार डाल कर अपने आक्रमणकारी की ओर निहारा परवेज ने। अब वहां गुस्से की जगह शरम ने ले ली थी। पारू को भी लगा, अब मैदान छोड़ देना ही ठीक है। पर जाते-जाते आखिरी गोला दागना नहीं भूली थीं वे। दरवाजे पर पहुंच, एक आखिरी नजर परवेज पर डालते हुए बोलीं, ‘‘कोई किसी के लिए नहीं मरता डाॅक्टर साहेब, ना ही मरने में कुछ रखा है। बात तो तब है, जब किसी के वास्ते जिया जाए।’’
लेकिन जिंदगी की ओर तकने की ज्यादा मोहलत ना परवेज खान को मिली, ना ही पारोमिता बनर्जी को। नीलमणि बनर्जी को अचानक दिल का दौरा पड़ा। इलाज के लिए कलकत्ते ले जाना पड़ा, और पूरा परिवार साथ हो लिया। कलकत्ता ने नीलमणि को वापस ढाका नहीं जाने दिया, ईश्वर के पास भेज दिया। पारू की मां ने वहीं अपने 2 बड़े बेटों के साथ ही रहने का निश्चय किया। ठीक भी था, अनजान शहर, अनजान लोगों के बीच बूढ़ी दीदी मां और 3 युवा होते बच्चों के साथ कैसे रहतीं वे। बचपन ही की तरह 16 बरस की पारू से किसी ने नहीं पूछा, ना वे कह पायीं कि उनका घर छूटा जा रहा है। साथ ही आने वाली जिंदगी का वह सपना भी, जिसे वे पूरी तरह देख भी नहीं पायी हैं।
कलकत्ता में कॉलेज में दाखिला ले लिया पारू ने, और ढाका की यादें फहमीदा को लिखी चिट्ठियों में सिमट गयीं। फहमीदा के हर खत में परवेज का जिक्र होता। ‘‘भाई को डॉक्टरी में गोल्ड मेडल मिला, भाई आगे की पढ़ाई के लिए लंदन जा रहे हैं...’’ आदि-आदि। कहीं ना कहीं शायद पारू भी समझ गयी थीं कि उनकी सहेली की चिटि्ठयां जो जानना चाहती हैं, साफ-साफ पूछ नहीं पातीं। इसीलिए वे हर तफसील बिना पूछे ही लिख देती थीं। और जो कुछ वे नहीं लिख पायीं, परवेज ने एक दिन हिम्मत करके खुद ही लिख डाला।
‘‘मैं तुम्हें बहुत याद करता हूं पारू... हर पल तुम्हारी खैरियत की दुआ करता हूं। तुम आगे पढ़ रही हो, जान कर खुशी हुई। शायद इन किताबों में तुम्हें अपने सवालों के जवाब मिल जाएं। कभी-कभी लगता है तुम पारोमिता ना हो कर परवीन या जन्नत होतीं, तो खतों के बजाय अम्मी को कह कर शादी का पैगाम भेज देता। मैं अब्बू से अब भी बात कर सकता हूं, पर वे भी मेरी तरह मजबूर हो जाएंगे। तुम्हारी मां और दीदी मां हमें समाज से अलग-थलग होते नहीं देख पाएंगी। हमारे रिश्ते में प्यार की जगह मजबूरियां और दुराव-छिपाव हावी हो जाएंगे। समझौते रह जाएंगे, प्यार नहीं। मैं अगले महीने लंदन जा रहा हूं। जिन बीमारियों का इलाज ढूंढ़ा जा सकता है, जरूर ढूंढ़ने की कोशिश करूंगा। और जो कुछ भी लाइलाज है, दुआ करूंगा कि उनके हल भी जल्द से जल्द मिल जाएं।’’
आगे के शब्द पारू के आंसुओं में घुल कर धुल गए थे। दीदी मां ने काफी दिनों से पारू की मां को चेताना शुरू किया था, उनके विवाह के बारे में। सो वह भी जल्दी ही हो गया। सोमेश्वर भट्टाचार्य हर लिहाज से आदर्श पति साबित हुए। समृद्ध घर-खानदान, पढ़ाई-लिखाई, तहजीब-तमीज से लबरेज। बड़ी बात यह थी कि पारू को भी उन्होंने अपनी चुनी राह पर चलने की हर संभव आजादी दी। पारोमिता भट्टाचार्य ने एमए तक पढ़ाई भी की, गृहस्थी की जानलेवा जिम्मेदारियों से यथासंभव मुक्ति पायी, और यहां तक कि कभी कुछ नहीं भी बताना चाहा सोमेश्वर को, तो उन्होंने बताने को मजबूर नहीं किया। ऐसे साधु व्यक्ति को पति रूप में पा कर पारोमिता को कभी-कभी ईश्वर की सत्ता पर विश्वास हो ही जाता था। और यह विश्वास और मजबूत हुआ था शुभोजित को पुत्र रूप में पा कर।
भावनासंपन्न मां का बुद्धिजीवी पुत्र था शुभो। मां के हर विचार, हर इच्छा को मान दिया था उसने। केवल यह जान कर कि पारोमिता अब दोबारा बंगाल की धरती नहीं छोड़ना चाहेंगी, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी की नामी फेलोशिप छोड़ कलकत्ता में ही घर बनाया था उसने। साॅल्ट लेक का वह फ्लैट खूबसूरत तो था ही, यह जान कर कि वह केवल पारोमिता की भावनाओं को समर्पित है, पारू की नजर में अनमोल हो जाता था। बहू लतिका भी अमेरिका में पढ़ी-लिखी अभिजात्य महिला थी। पति और सास की इस भावनात्मक ‘टयूनिंग’ पर कभी सवाल नहीं उठाए थे उसने। यही देख कर पारू उसकी बेहद कृतज्ञ हो उठती थीं। आज भी मां को अन्यमनस्क देख कर शुभो काफी देर पारू के पलंग के पास कुर्सी डाल कर बैठा रहा।
कुछ देर बाद पारू की नींद टूटी, तो पाया कि शुभो उन्हीं को एकटक देख रहा है।
‘‘तुम गए नहीं बेटा?’’
‘‘नहीं मां... तबीयत ठीक है अब?’’
‘‘हां, तबीयत को क्या होना है?’’

‘‘जुलूस देख कर बहुत घबरा गयी थीं ना, इसीलिए पूछ रहा हूं।’’
‘‘हां शुभो... हालांकि कोई पहला या आखिरी जुलूस तो नहीं है, जो इस तरह घबराऊं।’’
‘‘आपको परेशान कर देता है ना यह हिंदू-मुस्लिम विवाद? पर मां, अब तो यह रोजमर्रा का हिस्सा बनता जा रहा है।’’
‘‘शुभो, इतनी उम्र बिना विवाद देखे गुजरी हो, ऐसा नहीं। पर इतना जहर, इतनी नफरत देख कर लगता है, आजादी के इतने वर्ष क्या किया हमने?’’
‘‘मां, हमारी उदारता को हमारी कमजोरी समझ लिया जाता है।’’
‘‘हां, लेकिन उदार ना रह कर असहिष्णु हो जाना, जानलेवा हमलों पर उतर आना, यह कैसी ताकत है?’’
‘‘मां, जो लोग विवाद के बीचोंबीच होते हैं, वे सब कुछ भुगतते भी हैं, और वैसे ही उत्तर देते हैं। हम-तुम तो महज दर्शक हैं, बाहर के लोग।’’
‘‘विवाद का मर्म समझो शुभो। किसी ने क्या खाया, क्या पहना, क्या कहा, यह हमले या हत्या का विषय क्यों बनता है? विवाद पैदा नहीं होते, पैदा किए जाते हैं, उन्हें हवा दी जाती है, और उनके निष्कर्षों को अपनी सुविधानुसार तोड़ा-मरोड़ा जाता है। विवाद पहले भी एक छोटे तबके द्वारा बड़े जनसमूह को काबू करने का हथियार थे, आज भी हैं। कोई नहीं समझता कि नुकसान किसका होता है, और कितना?’’
शुभो एकटक देख रहा था मां की ओर। बंगला साहित्य में पोस्ट ग्रेजुएट हैं पारोमिता, िफर सामाजिक अर्थ-अनर्थ पर इतनी समझ कहां से पायी उन्होंने।
पारू कहती रहीं... ‘‘प्रजातंत्र की सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि यह समूह की ताकत से चलता है। उस समूह में जन की असली ताकत कहीं खो जाती है। सामाजिक संस्थाएं विकृत होती चली जाती हैं और समाज का स्वरूप भयावह हो जाता है। जनमानस को जब तक यह बात समझ जाती है, पछतावे की घड़ी बीत चुकी होती है।’’
शुभो ने पारू को फिर से पलंग पर लिटा दिया।
‘‘आप थक जाएंगी, मां। समझ रहा हूं आपकी बात। पर ऐसी चेतना आते समय लगेगा हमें। काफी युवा प्रजातंत्र है हमारा, एक तरह से शैशवकाल में। इसे विसंगतियों से ऐसे ही जूझना होगा, प्रौढ़ और समृद्ध होने से पहले।’’
पारोमिता मन ही मन शांत हुईं। शुभोजित की बातों में एक पुरानी छवि उभरी, शांत, संयत, समझदार। परवेज खान के खत का अर्थ भी शायद यही था। समाज के विरुद्ध जा कर एक-दूसरे को अपनाने से एक-दूजे को ही खो बैठते शायद। परवेज की समझ को शायद उसी पल अपने दिल के गर्भगृह में छुपा लिया था पारू ने। उसी में से जन्मा है सामने बैठे पुरुष का अक्स। उसमें पारू के लिए भी स्थान है, लतिका के लिए भी, आसपास निरंतर उभरती शांत-अशांत विचारधाराओं के लिए भी। वह इस नीड़ को बिखरने नहीं देगा, यह सोच कर पारू को लगा, उनका प्रेम व्यर्थ नहीं गया। वह तो इसी हवा में सांस ले रहा है, और नीलकंठ की तरह सारा विष पी लेगा, ताकि पारोमिता सुख की नींद सो सकें।
शुभोजित ने उठ कर खिड़की दोबारा खोल दी। बाहर वातावरण भी शांत था, और हवा भी।